दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मामले पर केंद्र का रवैया निराशाजनक
हमारे देश का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, जिसकी नींव संविधान और विधि के शासन पर टिकी हुई है।

बलदेव राज भारतीय
देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सच्चा देशभक्त मानता है। वह राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों पर बड़े ज्ञानवर्धक विचार प्रकट करता है और देश में फैले भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बेईमानी व रिश्वतखोरी पर कठोर आक्रोश व्यक्त करता है, मानो उससे बड़ा राष्ट्रहितैषी कोई और नहीं। किन्तु, विडंबना यह है कि उसे ये सारी बुराइयाँ केवल दूसरों में ही दिखाई देती हैं, स्वयं में नहीं। वह अपने आपको ईमानदार, सत्यनिष्ठ, निष्कलंक और आदर्शवादी मानता है, जबकि उसके विचार और कर्म प्रायः इसके विपरीत होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लोग अपने दोहरे मापदंडों के कारण राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जिस नैतिकता की अपेक्षा दूसरों से रखते हैं, उसी को अपने आचरण में अपनाने से कतराते हैं।
हमारे देश का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, जिसकी नींव संविधान और विधि के शासन पर टिकी हुई है। यह प्रणाली नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देती है। लेकिन जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं और कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो यह व्यवस्था के मूल्यों पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगा देता है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि दागी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने की मांग पर विचार होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। यह विवाद एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है—क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए? या उन्हें संसद और विधानसभाओं में भेजकर कानून बनाने की शक्ति दे देनी चाहिए?
लोकतंत्र का आधार 'जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार' की अवधारणा पर टिका होता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को मताधिकार और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नागरिक, जब तक वह कानूनी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, चुनाव लड़ सकता है और जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि, यदि जनता के प्रतिनिधि स्वयं गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हों, तो क्या वे समाज में कानून और न्याय की स्थापना कर सकते हैं? संविधान का उद्देश्य योग्य, ईमानदार और जनसेवा को समर्पित लोगों को शासन में शामिल करना है, न कि वे लोग जो स्वयं कानून तोड़ते हैं।
आज चुनाव लड़ना गरीब व्यक्ति के लिए एक असंभव सपना बन गया है। गांव की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई, पंचायत, में सरपंच बनने के लिए भी प्रत्याशी लाखों रुपये खर्च करते हैं, तो विधायक और सांसद बनने के लिए करोड़ों की जरूरत होती है। धन के अभाव में एक आम नागरिक चाहकर भी चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकता।
इसके विपरीत, अपराधी प्रवृत्ति के लोग भ्रष्टाचार और अवैध साधनों से अर्जित धन के बल पर न केवल चुनाव लड़ते हैं, बल्कि जेल में रहते हुए भी जीत हासिल कर लेते हैं। विडंबना यह है कि गरीब और शोषित वर्ग, जो स्वयं व्यवस्था परिवर्तन का इच्छुक होता है, भय और दबाव में आकर ऐसे दागी प्रत्याशियों को ही अपना नेता चुन लेता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के मूल्यों को क्षीण कर रही है और चुनावी प्रक्रिया को धनबल एवं बाहुबल का खेल बना रही है।
देश में कई ऐसे राजनेता हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 43% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें से कई संगीन अपराधों से जुड़े थे, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण और भ्रष्टाचार। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाता है, बल्कि जनता का विश्वास भी कम करता है। यदि कोई आम नागरिक मामूली अपराध में भी दोषी पाया जाता है, तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। वहीं, जिन पर हत्या, दंगा और घोटालों के आरोप हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं और संसद या विधानसभा का हिस्सा बन सकते हैं। यह असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी राजनीति में आपराधिक तत्वों की भागीदारी को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर दागी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया गया, तो यह विधायिका को कमजोर कर देगा और कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यह तर्क कुछ गले से नहीं उतरता। क्या अपराधी लोगों को राजनीति में रोकने से राजनीति गंदा होने से नहीं बचेगी? अपराधी प्रवृत्ति के लोग किस प्रकार के कानून का समर्थन करेंगे, यह जगजाहिर है।
सत्य यही है कि केंद्र सरकार का यह तर्क लोकतंत्र की भावना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। संसद और विधानसभा में बैठने वाले प्रतिनिधियों का नैतिक और कानूनी रूप से स्वच्छ होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है, तो उसे जनता की सेवा करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मिल भी कैसे सकता है, जो स्वयं अपराधी हो वह समाज सेवा कैसे कर सकता है।
आजीवन प्रतिबंध लगाने का विरोध करने वाले यह तर्क देते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुका है, तो उसे पुनः समाज में योगदान देने का अवसर मिलना चाहिए।
लेकिन, राजनीति कोई साधारण नौकरी नहीं है; यह देश और समाज की सेवा का एक पवित्र कार्य है। यदि सरकारी सेवाओं में नौकरी करने के लिए किसी व्यक्ति का चरित्र प्रमाणपत्र आवश्यक होता है, तो विधायिका में प्रवेश के लिए भी नैतिकता और कानूनी स्वच्छता की कसौटी होनी चाहिए।
चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, जिससे वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर सख्त निर्णय ले सके। ऐसे नेताओं पर चलने वाले मामलों को विशेष न्यायालयों में रखा जाए, ताकि फैसले शीघ्रता से हों और दोषी पाए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सके। नेताओं के लिए शिक्षा, ईमानदारी और नैतिकता को अनिवार्य किया जाए। जो नेता स्वयं ईमानदार और देश और संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं होगा तो वह जनता के लिए कैसे और किस प्रकार आदर्श सिद्ध हो सकता है।
चुनाव आयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं मतदाताओं को जागरूक करें कि उन्हें बिना किसी लालच में आए स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को ही चुनना चाहिए। जो भी उम्मीदवार या दल उन्हें किसी प्रकार का लालच या प्रलोभन दें उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करें।
लोकतंत्र की सफलता उसके नेताओं की स्वच्छता और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। यदि राजनीति अपराधियों का अड्डा बन जाएगी, तो यह पूरे शासन तंत्र को भ्रष्ट कर देगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि दागी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे और जनता का विश्वास मजबूत हो।
स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।
About The Author
Related Posts
Post Comment
आपका शहर
 प्रधानमंत्री के सरकारी नौकरियों में चयनित 51000 से अधिक अभ्यर्थिंयों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का किया गया सजीव प्रसारण।
प्रधानमंत्री के सरकारी नौकरियों में चयनित 51000 से अधिक अभ्यर्थिंयों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का किया गया सजीव प्रसारण। अंतर्राष्ट्रीय
 सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इंडो-नेपाल बॉर्डर एरिया में गतिविधियों पर रखी जा रही है सतर्क दृष्टि
सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इंडो-नेपाल बॉर्डर एरिया में गतिविधियों पर रखी जा रही है सतर्क दृष्टि Online Channel
खबरें
शिक्षा
राज्य

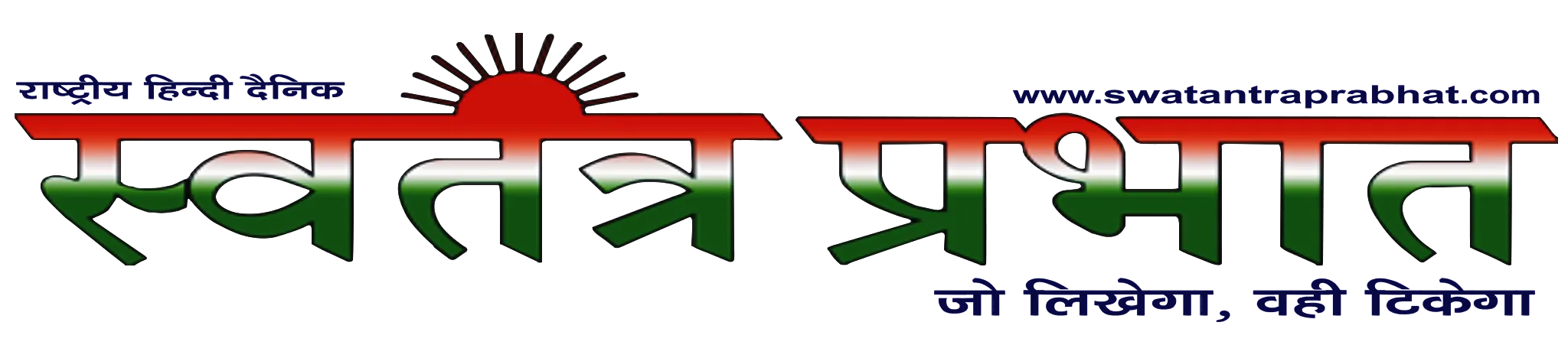









.webp)

2.jpg)
3.jpg)

















1.jpg)









Comment List