रेडियो: हर हृदय की धड़कन, हर दौर की आवाज़
[जब शब्द सीमाएँ लांघे, तब रेडियो जनमानस गढ़े]
.jpg)
रेडियो केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि संवाद, संस्कृति और जनचेतना की सजीव ध्वनि है। जब भी यह बोलता है, तो सिर्फ तरंगें नहीं गूंजतीं, बल्कि भावनाएँ जागती हैं, विचार प्रवाहित होते हैं और समाज के हर कोने तक चेतना का संचार होता है।
संचार की इस सशक्त विधा ने हर युग में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है—चाहे वह संघर्ष के दिन हों या उत्सव की घड़ियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ हों या सामाजिक बदलाव की लहर। जब अखबारों की पहुँच सीमित थी, जब टेलीविजन आम आदमी की पहुंच से दूर था, तब रेडियो ही था जिसने हर घर तक समाचार, संगीत और संवाद की अलख जगाई।
यह महज़ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक क्रांति की आवाज है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर डिजिटल युग तक अपना लोहा मनवाया है। वक्त बदला, तकनीक उन्नत हुई, लेकिन रेडियो की आत्मीयता और प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। इसकी धुनें आज भी वही अपनापन लिए बहती हैं, जो दिलों को जोड़ने और विचारों को जगाने की ताकत रखती हैं।
रेडियो का इतिहास एक स्वर्णिम यात्रा की भांति है, जिसने संचार के नवीन आयाम गढ़ते हुए समूचे विश्व को जोड़ने का कार्य किया। 1895 में गुग्लिएल्मो मारकोनी के आविष्कार ने संवाद की एक क्रांतिकारी विधा को जन्म दिया, जो कालांतर में मानव सभ्यता की अभिव्यक्ति और संपर्क का सशक्त माध्यम बनी।
भारत में रेडियो का उद्घाटन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में हुआ, किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसे बंद करना पड़ा। 1936 में "ऑल इंडिया रेडियो" (आकाशवाणी) का जन्म हुआ, जो कालांतर में राष्ट्र की सशक्त वाणी बनकर उभरा।
1957 में "आकाशवाणी" के रूप में इसे एक नवीन पहचान मिली, जिसने बहुरंगी भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधते हुए संस्कृति, सूचना और मनोरंजन का सेतु निर्मित किया। इसकी अभूतपूर्व भूमिका को सम्मानित करने हेतु 2011 में यूनेस्को ने 13 फरवरी को "विश्व रेडियो दिवस" घोषित किया, जिससे इस माध्यम की वैश्विक प्रासंगिकता और महत्ता को चिरस्थायी मान्यता प्राप्त हुई।
रेडियो की सबसे विलक्षण विशेषता इसकी असीमित पहुंच और सहजता है। यह किसी इंटरनेट कनेक्शन या महंगे उपकरणों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि एक साधारण ट्रांजिस्टर या मोबाइल में भी अपनी पूरी ऊर्जा और स्पष्टता के साथ गूंजता है। यह मात्र एक संचार माध्यम नहीं, बल्कि शब्दों की वह सशक्त धारा है,
जो भाषा, जाति, वर्ग या भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर हर हृदय तक अपनी अनुगूंज पहुंचाती है। दूरस्थ गाँवों की पगडंडियों से लेकर अट्टालिकाओं से घिरे महानगरों तक, किसानों के लहलहाते खेतों से लेकर शहरों की चहल-पहल भरी गलियों तक, रेडियो अपनी अमिट छाप छोड़ता है।
जब विपदाएँ दस्तक देती हैं, अखबारों की छपाई ठहर जाती है, टेलीविजन नेटवर्क बाधित हो सकते हैं, किंतु रेडियो अविराम सत्य की गूंज बनकर संचार का सेतु बना रहता है। 2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी और हाल के वैश्विक संकटों में इसकी अपरिहार्यता प्रमाणित हो चुकी है। यह न केवल संकट के समय संजीवनी बनकर मार्गदर्शन करता है, बल्कि शांति के समय संस्कृति, संस्कार और सजीव परंपराओं को संजोने वाला अमर माध्यम भी है।
रेडियो केवल सूचनाओं और समाचारों का स्रोत मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा, ज्ञान और मनोरंजन का अनूठा संगम है। इसकी तरंगों में वह जादू है, जो श्रोताओं की संवेदनाओं को छूकर उनके हृदय में गूंज बनकर बस जाता है। यह लोकगीतों की मधुरता से लेकर आधुनिक संगीत की धुनों तक, हास्य के चटपटे रंगों से लेकर गूढ़ विमर्शों तक, हर वर्ग, हर रुचि और हर पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ संजोए रखता है। इसकी व्यापक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता ने इसे जनसंवाद और राजनीति के लिए भी एक सशक्त मंच बना दिया।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में "मन की बात" कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसने सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर रेडियो की प्रासंगिकता को एक नई ऊँचाई प्रदान की। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, बल्कि आम नागरिकों की प्रेरणादायक कहानियाँ साझा कर समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आशा का संचार किया जाता है। "मन की बात" ने रेडियो को पुनः संवाद और संप्रेषण के केंद्र में स्थापित कर दिया है।
तकनीकी क्रांति के इस युग में, जहाँ इंटरनेट और डिजिटल मीडिया नए आयाम गढ़ रहे हैं, रेडियो ने भी स्वयं को समय के साथ ढालते हुए अपनी चमक बनाए रखी है। एफएम रेडियो, इंटरनेट रेडियो और पॉडकास्ट जैसे आधुनिक स्वरूपों ने इसकी लोकप्रियता को नए पंख दे दिए हैं।
अब रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से भी सहजता से सुना जा सकता है, जिससे इसकी पहुँच और प्रभाव पहले से कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली हो गया है। परंतु माध्यम चाहे कोई भी हो, रेडियो की आत्मा सदैव एक ही रही है—जनता की आवाज, संस्कृति का प्रहरी और संवाद का सबसे प्रभावी और जीवंत जरिया।
रेडियो मात्र अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की अपरिहार्य आवश्यकता भी है। यह केवल ध्वनि की तरंगें नहीं, बल्कि समाज की धड़कन, विचारों की ऊर्जा और जनभावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जो न केवल सुनने, बल्कि सोचने, समझने और जागरूक होने की दिशा में प्रेरित करता है। बीते युगों में इसने क्रांतियों को स्वर दिया,
आज यह बदलाव की लहरों को दिशा दे रहा है, और आने वाले समय में भी संवाद, सशक्तिकरण और मानवीय संवेदनाओं की अमिट आवाज बना रहेगा। जब तक इस संसार में विचारों का आदान-प्रदान आवश्यक रहेगा, तब तक रेडियो की स्वरलहरियाँ भी अनवरत, अविराम और अडिग रूप से गूंजती रहेंगी, हर हृदय तक अपनी अनुगूंज पहुँचाती रहेंगी।
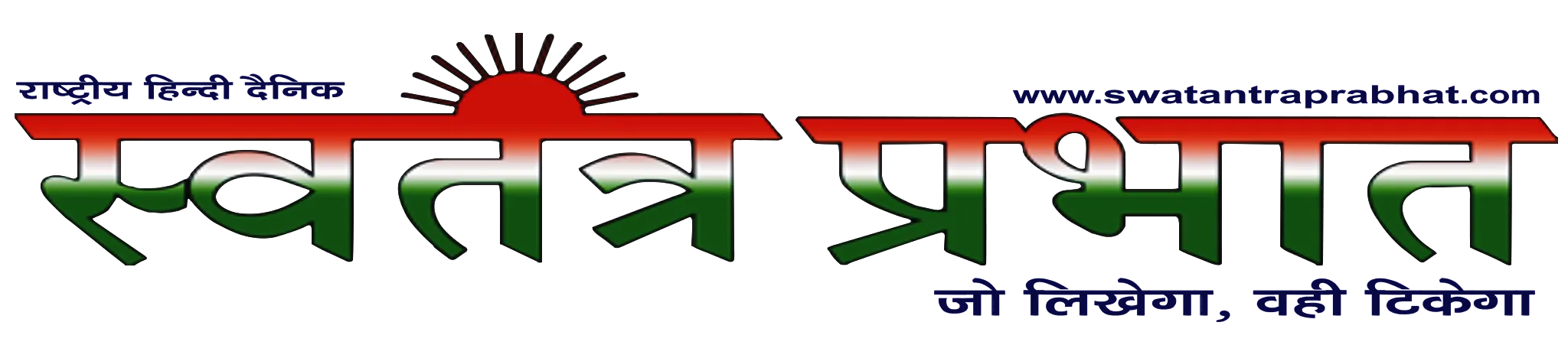








.jpg)

.jpg)







.jpg)
.jpg)

.jpg)
1.jpg)

.jpg)



.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

Comment List